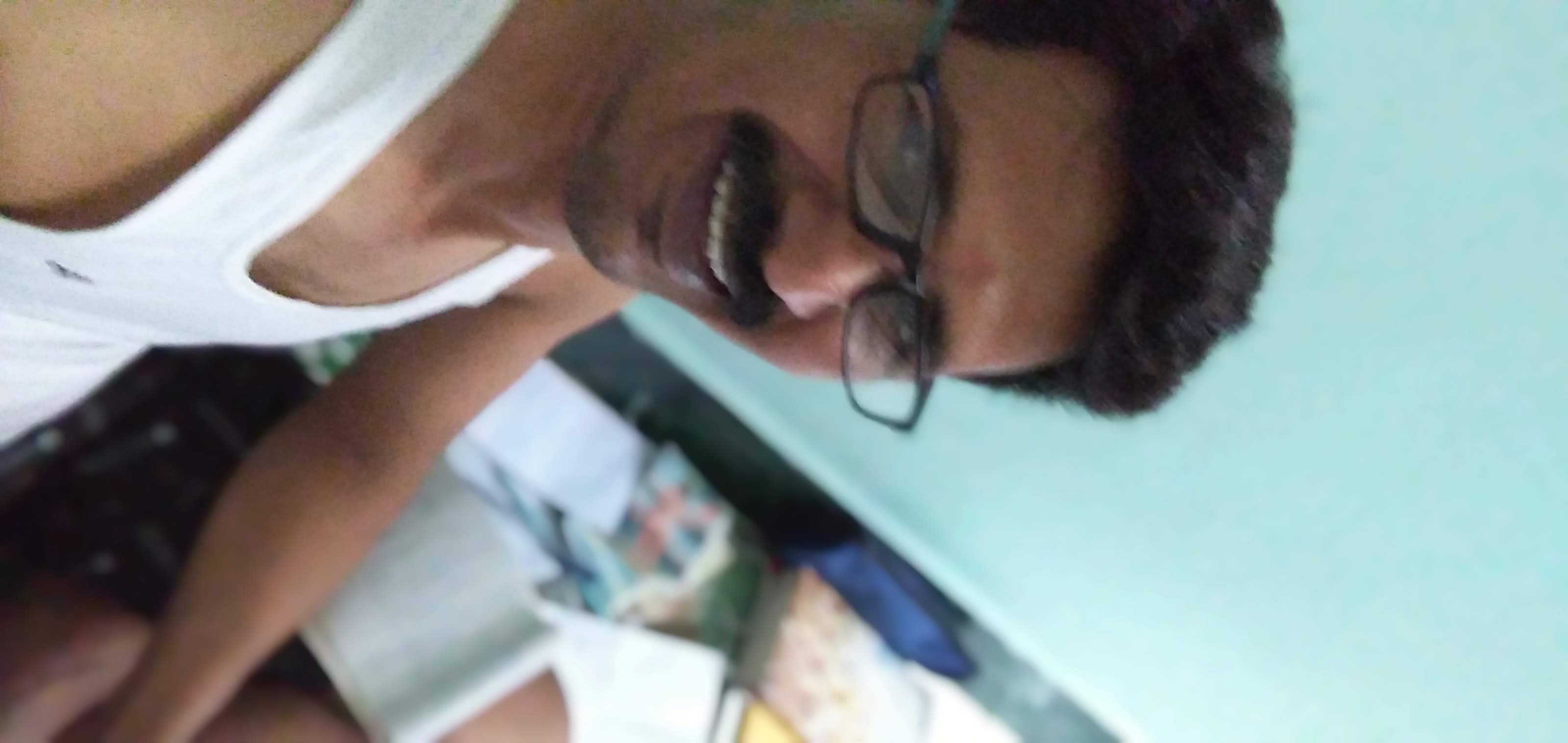नानी का एक संदूक था —
लकड़ी का,
बड़े ताले वाला,
जिसे खोलते समय
ऐसा लगता था
जैसे कोई पुराना मंदिर
धीरे से साँस ले रहा हो।
मैं बच्ची थी —
सिर्फ़ देख सकती थी,
छू नहीं सकती थी।
पर एक दिन
नानी ने धीरे से कहा,
“आ, आज तुझे कुछ दिखाऊँ…”
उस दिन
पहली बार
संदूक खुला —
और उसमें सिर्फ़ कपड़े नहीं थे।
वो एक पूरा जीवन था —
सिलवटों में छिपा हुआ।
पुरानी साड़ियाँ थीं —
हर साड़ी के साथ एक कहानी।
“ये तेरे नाना के पहले वेतन पर आई थी…”
“ये मैं तेरी माँ के जन्म के बाद पहनी थी…”
“इसमें मैं पहली बार मंदिर गई थी…”
“इसमें मैं पहली बार टूटी थी।”
एक कोने में
कुछ चिट्ठियाँ थीं —
जिनमें नानी ने कभी जवाब नहीं लिखा था।
एक सुई-धागे की डिब्बी थी —
जो रिश्तों को भी सीने का हुनर जानती थी।
एक छोटा आईना था —
जो नानी के चेहरे की
हर झुर्री जानता था,
हर आँसू देख चुका था,
पर कभी किसी से कुछ नहीं बोला।
उस दिन मैं समझ गई —
स्त्रियाँ अपने भीतर
कितने संदूक छुपा कर जीती हैं,
जिनमें वे अपनी हँसी, आंसू,
अधूरे गीत, पुराने ज़माने की महक
सब बंद कर देती हैं।
सालों बाद
जब नानी नहीं रहीं,
तो सबने कहा —
“संदूक बेकार हो गया है,
कपड़े बाँट दो… फेंक दो…”
मैंने कुछ नहीं कहा।
बस रात में
वहीं संदूक के पास बैठकर
धीरे से
उस आईने में खुद को देखा…
और जाना —
अब मैं भी
एक संदूक बन रही हूँ।
कुछ संदूक
ताले से नहीं,
स्मृतियों से बंद होते हैं।
और उनमें रखी कहानियाँ
सिर्फ़ स्त्रियाँ पढ़ सकती हैं —
वो भी मौन में।”



 The Flower of Word by Vedvyas Mishra
The Flower of Word by Vedvyas Mishra The novel 'Nevla' (The Mongoose) by Vedvyas Mishra
The novel 'Nevla' (The Mongoose) by Vedvyas Mishra The Flower of Word by Vedvyas Mishra
The Flower of Word by Vedvyas Mishra