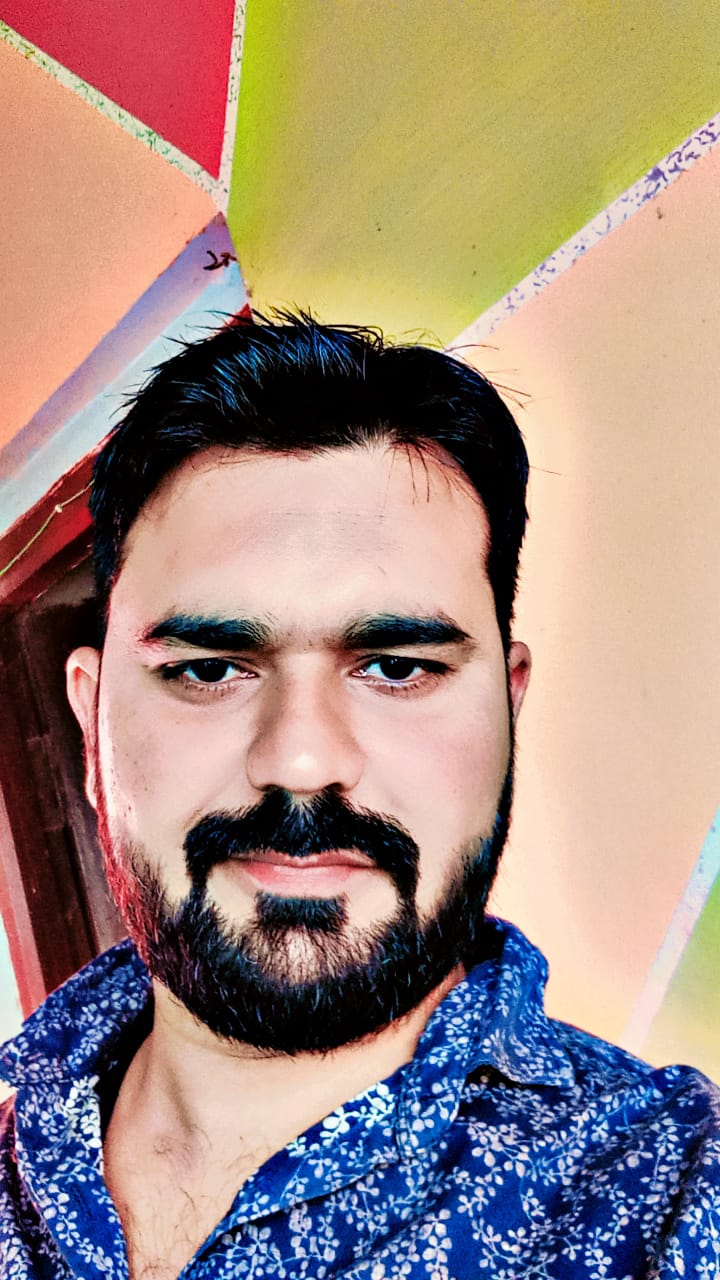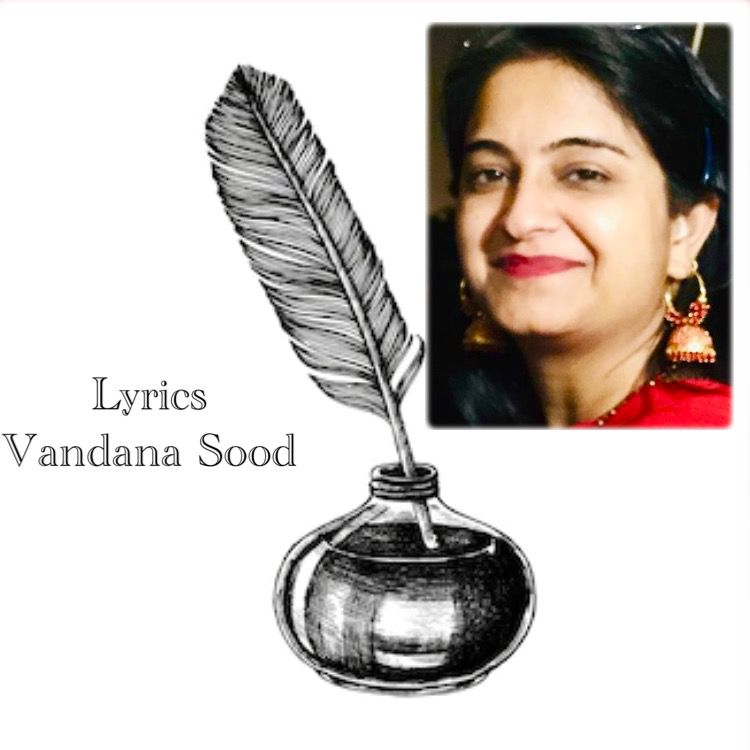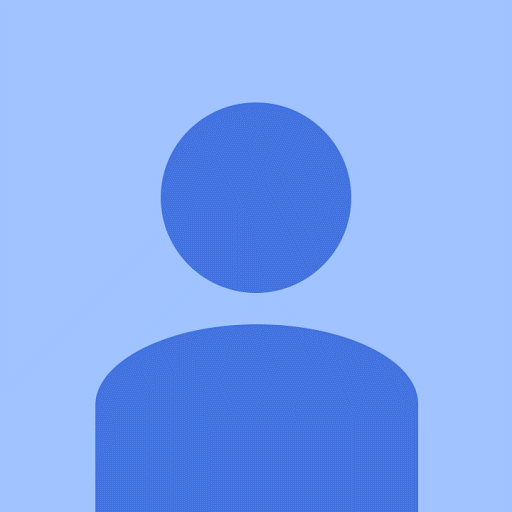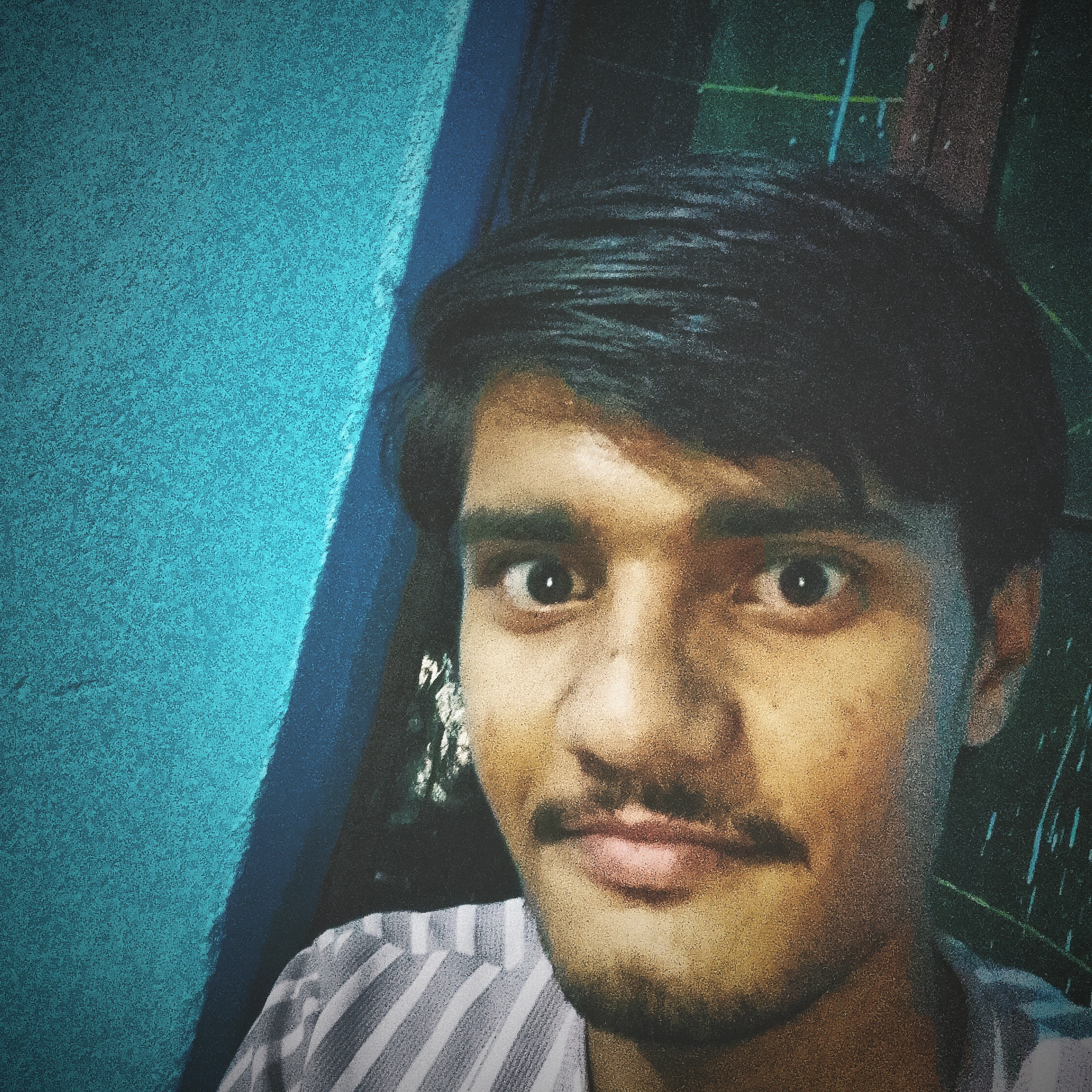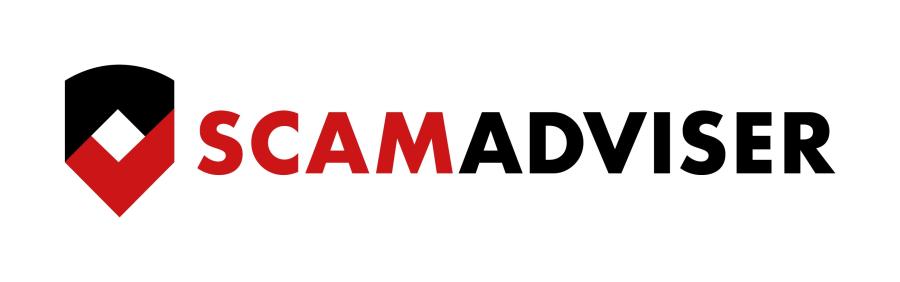उपभोक्तावादी संस्कृति और बाजार के विस्तार ने आवश्यकताओं के स्थान पर लालच और दिखावे के उपभोग को महत्त्वपूर्ण बना दिया है। इसलिए बाजारवादी शक्तियां बच्चों के सामने उत्पन्न संकट की स्थितियों को भी एक व्यावसायिक अवसर के रूप में ही देखती हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि बच्चे समय से पहले ही बड़े हो रहे हैं।
आज के उपभोक्तावादी समाज में हर वस्तु बिकाऊ बना दी गई है। कहा जाता है कि बाजार का केवल एक नियम होता है कि बाजार का अपना कोई नियम नहीं होता। इसलिए हर चीज, यहां तक कि भावना और रिश्ते भी उपभोग की वस्तु बन चुके हैं। जिसे मन चाहा, दाम लगा कर बेचा और खरीदा जा सकता है। दुनिया तेजी से बदल रही है, इसलिए परिवार, शिक्षा, राजनीति और अर्थव्यवस्था भी समय के अनुरूप तेजी से करवटें ले रही हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं कि तेजी से बदलते इस दौर ने मनुष्य की उम्र के हर पड़ाव को प्रभावित किया है। अगर बाल्यावस्था की बात करें, तो बचपन खो गया है या कहें कि आज के दौर में बचपन जैसा कुछ रह ही नहीं गया। बच्चे सीधे किशोर या युवावस्था में कदम रखने लगे हैं। अब बच्चे खिलौनों से नहीं, मोबाइल और कंप्यूटर से खेलते हैं, इसलिए वे वास्तविक विश्व और समाज का हिस्सा नहीं बन पा रहे।
इसकी जगह आभासी समाज ने ले ली है। कंप्यूटर गेम की इस दुनिया ने उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल दिया है। किशोर आबादी कंप्यूटर गेम, गैजेट, सोशल मीडिया आदि में उलझ कर रह गई है। यह सब बाजारवाद और उपभोक्तावाद का परिवार और समाज पर बढ़ते प्रभाव का ही नतीजा है।
बाजार का एकमात्र लक्ष्य अधिक से अधिक लाभ कमाना ही होता है। इसके लिए वह मनुष्य की भावनाएं, रिश्ते, दुख-दर्द, खुशी सबका कारोबार करता है। हाल में छपी एक खबर के अनुसार जापान के एक अरबपति ने इंसानी भावनाओं को समझने और उनका अकेलापन दूर करने वाले रोबोट बनाने वाली कंपनी में निवेश किया है।
इस उत्पाद का नाम लोवोट है जो लव और रोबोट से मिल कर बना है। उनका दावा है कि यह रोबोट इंसान की हर भावना को समझने और उन्हें खुश और स्वस्थ रखने में सक्षम है। उनका तर्क है कि कोरोना काल में इस तरह के रोबोट ने बीमार लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाई। सच भी है कि जब समाज में मनुष्य की भूमिका पर सवाल उठने लगे या वह अपनी भूमिका निभाना छोड़ दे, तो मशीनों द्वारा इंसानों को विस्थापित करना कहीं न कहीं एक मजबूरी भी लगने लगती है।
केवल इतना ही नहीं, लाभ का बाजार दिनोंदिन व्यापक होता जा रहा है। अब व्यक्ति के वे निजी क्षण भी बाजार का हिस्सा बन गए हैं, जो कभी उसके परिवार तक सीमित थे। फिल्मों और धारावाहिकों ने इस निजी जीवन को बाजार तक पहुंचाने में कम बड़ी भूमिका नहीं निभाई। अब अधिकांश शादियों से पहले महंगे-महंगे कपड़े पहना कर, महंगी-महंगी जगहों पर दूल्हा-दुल्हन के शादी पूर्व की फिल्में तक बनाई जाती हैं और इस तरह उन्हें उस आभासी दुनिया की सैर करवाई जाती है जिसका वास्तविक दुनिया से कोई सरोकार नहीं होता। और यह सफर केवल यहीं खत्म नहीं होता, फिर शादी समारोह आयोजित करवाने वाली प्रबंधन कंपनियां सक्रिय हो जाते हैं जो शादी को परी-लोक की कहानी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़तीं।
इसी तरह आजकल मातृत्व के दौरान की स्मृतियों को सहेजने के लिए ‘मैटरनिटी फोटोशूट’ का चलन भी तेजी से चल निकला है। पता ही नहीं चला कि वस्तुओं और सेवाओं को बेचते-बेचते कब भावनाओं का बाजार मूर्त रूप लेता गया। इस क्षणिक आनंद के लिए मनुष्य अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है, फिर उसे कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। क्योंकि उपभोक्तावादी समाज में इन सब दिखावों से ही किसी की प्रतिष्ठा का निर्धारण होता दिखता है।
उपभोक्तावादी संस्कृति और बाजार के विस्तार ने आवश्यकताओं के स्थान पर लालच और दिखावे के उपभोग को महत्त्वपूर्ण बना दिया है। इसलिए बाजारवादी शक्तियां बच्चों के सामने उत्पन्न संकट की स्थितियों को भी एक व्यावसायिक अवसर के रूप में ही देखती हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि बच्चे समय से पहले ही बड़े हो रहे हैं। संभवत: यही कारण है कि आए दिन ऐसी अनेक घटनाएं सामने आती हैं जिनमें बच्चे अपराधी की श्रेणी में खड़े नजर आते हैं।
सोशल मीडिया और कंप्यूटर खेलों के कारण पिछले कुछ वर्षों में बच्चों और किशोरों की आपराधिक गतिविधियों में सहभागिता तेजी से बढ़ी है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक वर्ष में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों में आठ सौ बयालीस हत्याएं, सात सौ पच्चीस अपहरण, छह हजार से ज्यादा चोरी, लूट और डकैती की घटनाएं शामिल हैं।
खेलने और पढ़ने की उम्र में बच्चों और किशोरों द्वारा इतने बड़े-बड़े अपराधों को अंजाम देना चिंता का विषय भी है और समाज के लिए बड़ी चुनौती भी। मोबाइल गेम में बड़ी रकम हार जाने पर अपने घर में चोरी, या अपहरण की कहानी गढ़ कर परिवारजनों से पैसे ऐंठना या फिर पैसों के लिए उनकी हत्या तक कर देना अब सामान्य अपराध हो गया है। लगता है, राज्य और समाज तो बच्चों के प्रति अपने दायित्व से मुक्त होकर दूर खड़ा तमाशा देख रहे हैं।
दुख की बात यह है कि शिक्षा भी इस दिशा में कोई महत्त्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रही है। परिवार और विद्यालय भी मूक दर्शक बन गए हैं। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक, स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम और देश व समाज के उत्थान के लिए एक समर्पित व मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण करना है। पर आज की शिक्षा उन्हें केवल प्रतियोगिता का हिस्सा बना रही है, क्योंकि इस प्रतियोगिता में विजयी होना ही उसके अस्तित्व की पहचान है।
इन प्रतियोगिताओं में जीत के लिए उन्हें विभिन्न शिक्षण उद्योगों में प्रवेश लेना जरूरी है, वरना उनकी हार सुनिश्चित है। ये शिक्षण और कोचिंग उद्योग सिर्फ अभिभावकों की खर्च करने की क्षमता देखते हैं, न कि बच्चों की रुचि या योग्यता। और यही एक बड़ी वजह है कि जो बच्चे इन प्रतियोगिताओं में पिछड़ जाते हैं या बिना इच्छा के इन प्रतियोगिताओं में धकेल दिए जाते हैं, वे जिंदगी से हार मानने लगते हैं। क्योंकि शिक्षा ने उन्हें यह नहीं सिखाया कि जिंदगी किसी एक प्रतियोगिता तक सीमित नहीं है, न ही जिंदगी दूसरों से प्रतिस्पर्धा का नाम है, बल्कि खुद को जीतना और खुद से जीतना जिंदगी है।
इस तरह के सामाजिक संकट के लिए परिवार भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। कुछ समाज वैज्ञानिक मानते हैं कि परिवार की अवधारणा में ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो परिवार को समाज विरोधी बनाते हैं। उनके अनुसार परिवार इसलिए समाज विरोधी है, क्योंकि यह महिलाओं के शोषण की वैधता को स्थापित करता है और यह परिवार के परिवेश के बाहर महिला के जीवन की किसी भी संभावना को समाप्त करता है।
विभिन्न विज्ञापनों और मीडिया में महिलाओं को सौंदर्य की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करना मुनाफे के बाजार को विस्तार देता है, न कि महिला सशक्तिकरण को। बाजार का चरित्र कल्याणकारी नहीं होता, बल्कि व्यक्तिवादी होता है, इसलिए लाभ कमाने के आलावा उसका कोई उद्देश्य नहीं होता।
बाजार की शक्तियां केवल मुनाफे के लिए काम करती हैं, इसलिए उनसे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन एक लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य, परिवार और शिक्षक समुदाय का ऐसे मुद्दों से मुंह मोड़ना समाज में उत्पन्न होने वाले जोखिमों की ओर संकेत करता है। अगर वर्तमान ऐसा है तो भविष्य की कल्पना कितनी भयावह होगी, कहने की आवश्यकता नहीं है। बाजार मानव आवश्यकताओं को पूरा करे, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर जरूरतों को निर्देशित और नियंत्रित करने लगे, तो वह समाज और राष्ट्र के लिए खतरा बन जाता है।
लेखक : ज्योति सिडाना

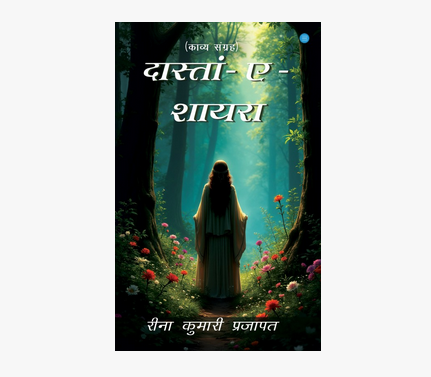

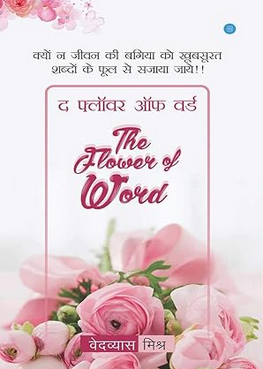 The Flower of Word by Vedvyas Mishra
The Flower of Word by Vedvyas Mishra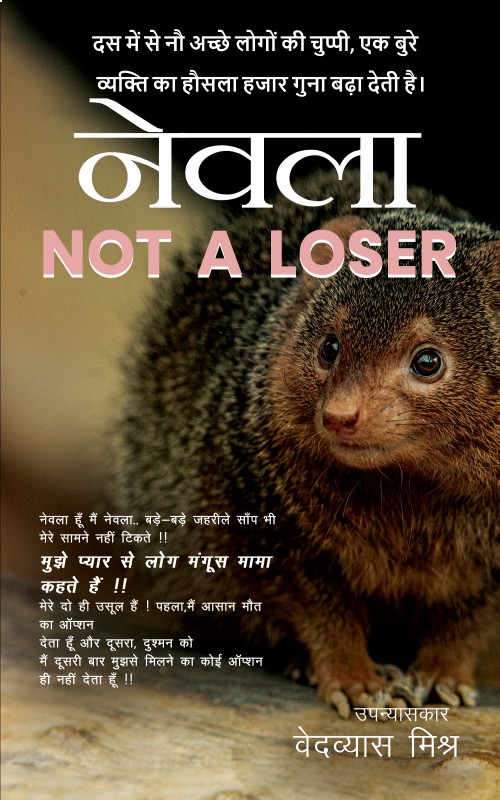 The novel 'Nevla' (The Mongoose) by Vedvyas Mishra
The novel 'Nevla' (The Mongoose) by Vedvyas Mishra The Flower of Word by Vedvyas Mishra
The Flower of Word by Vedvyas Mishra