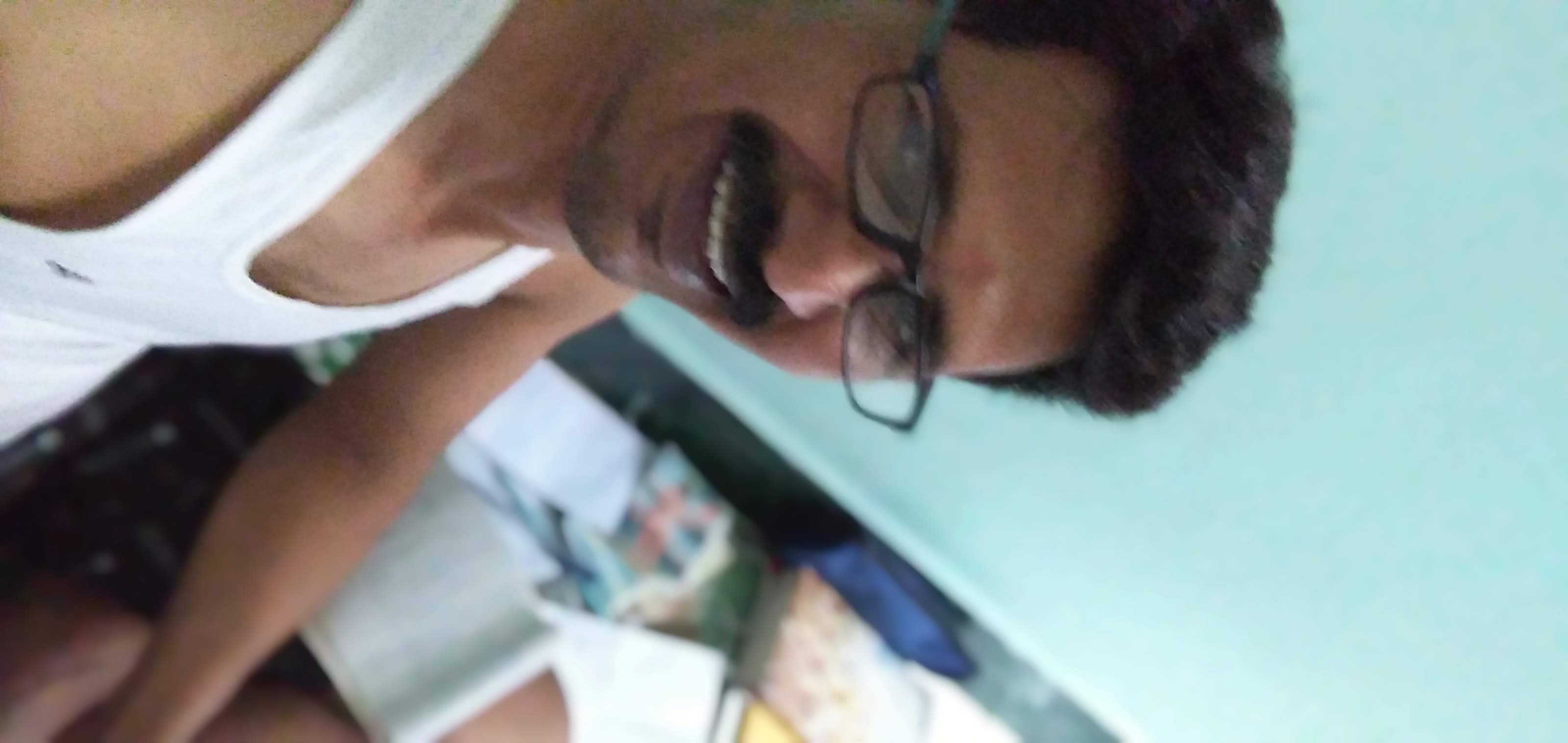बात छोटी थी, पर बढ़ गई,
तेरी आँखों की लौ बुझ गई।
मैं मनाने को तैयार खड़ा,
पर तेरी ख़ामोशी कुछ और कह गई।”
मैं लाया था,
तेरी पसंद की मिठाइयाँ,
कुछ पुराने किस्से,
दो-चार हँसी की पर्चियाँ,
पर तू चुप था—
जैसे सर्दियों में ठिठुरता कोई पेड़।
मैं बोला— “अरे, अब मान भी जा!
इतनी-सी बात पर इतना ग़ुस्सा?”
तेरी आँखों में हलचल हुई,
जैसे कोई तूफान थमने को था,
पर फिर ठहर गया,
फिर ठंडा हो गया,
जैसे कोई लावा, जो अंदर ही जम गया।
अब मैं उलझन में था—
तू रूठा था या टूटा था?
तेरी नाराज़गी थी या बेबसी?
तेरा ग़ुस्सा था या थकान?
अगर तू नाराज़ होता,
तो तर्क करता, बहस करता,
या फिर दरवाज़ा पटककर चला जाता।
पर तू बैठा था, चुपचाप,
अपनी ही सोचों में डूबा,
जैसे कोई ख़ुद से ही बात कर रहा हो।
मैंने तेरा हाथ थामा—
ठंडा था, भारी था,
जैसे किसी बूढ़े वटवृक्ष की जड़ें।
“सुन, मैं मान लूँगा कि ग़लती मेरी थी,
पर पहले ये तो बता,
तू मुझसे नाराज़ है,
या फिर… खुद से परेशान?”
तेरी साँसों ने भारीपन उगला,
तेरी आँखें पल भर को भीगीं,
फिर जैसे कोई दरवाज़ा खुला—
“ग़ुस्सा नहीं हूँ…
बस… थक गया हूँ…”
अब मैं समझ गया था,
ये रूठने का मामला नहीं था,
ये लड़खड़ाने का मामला था,
ये मनाने का नहीं,
साथ देने का मामला था।
इसलिए मैंने बहाने नहीं बनाए,
कोई मज़ाक नहीं किया,
बस पास बैठ गया,
तेरा हाथ अपने हाथों में लेकर—
बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने,
बस… तेरे साथ।
क्योंकि रूठों को मनाना आसान है,
पर जो अंदर से टूटा हो,
उसे बस…
समझने वाला चाहिए।



 The Flower of Word by Vedvyas Mishra
The Flower of Word by Vedvyas Mishra The novel 'Nevla' (The Mongoose) by Vedvyas Mishra
The novel 'Nevla' (The Mongoose) by Vedvyas Mishra The Flower of Word by Vedvyas Mishra
The Flower of Word by Vedvyas Mishra